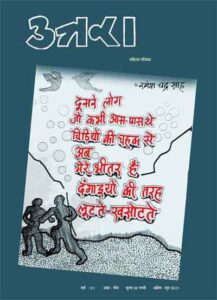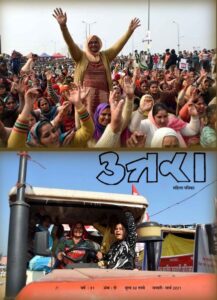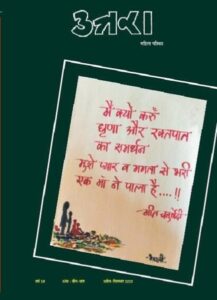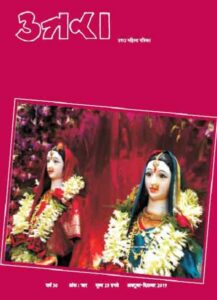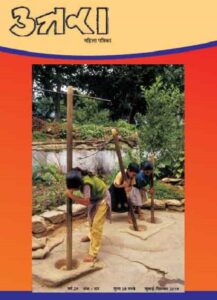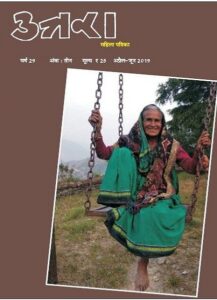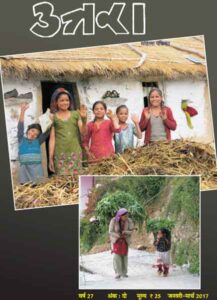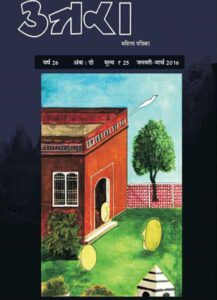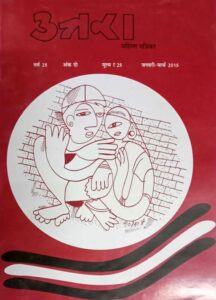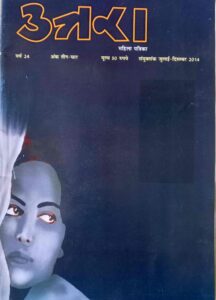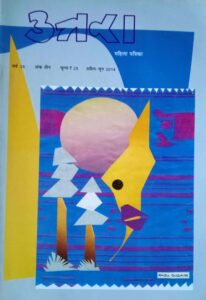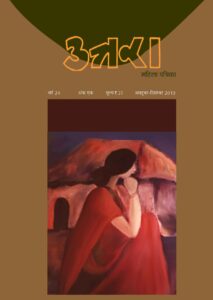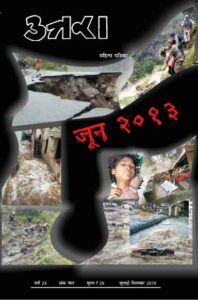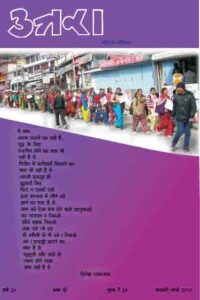नवजागरण, स्त्री प्रश्न और आचरण पुस्तकें
गरिमा श्रीवास्तव
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के पूवार्ध के भारत का राजनीतिक परिदृश्य जटिल और परस्पर विरोधी तत्वों से मिल कर बना था। समकालीन रचनाकारों की वैचारिकता के निर्माण में भाषिक, साम्प्रदायिक विमर्श और पितृसत्ता की भूमिका थी। वे सुधारोन्मुख दीखने के साथ-साथ औपनिवेशिक प्रभुवर्ग के हित-विरोधी भी नहीं दिखना चाहते थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जिस गद्य का निर्माण हो रहा था, वह उनके इस (एजेंडे) की पूर्ति में सहायक बना। उपन्यास-लेखन के प्रारम्भिक दौर में हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं के लेखक अपने-अपने समुदाय के भीतर स्त्रियों की दशा में सुधार की चिंता करते दिखने लगे। ब्रिटिश उच्चाधिकारियों की संस्तुति-प्रशस्ति और पुरस्कारों ने ऐसे गद्य-लेखन को प्रश्रय दिया जो उपन्यास के कलेवर में आचरण-संहिताएँ थीं। इस संदर्भ में यह आलेख मुख्यत: तीन प्रस्ताव करता है-
1. उपन्यास लेखन के प्रारम्भिक दौर में लिखी रचनाओं को न तो पूरी तरह पश्चिम से प्रभावित माना जाना चाहिए, न ही भारतीय आख्यान परम्परा से पूरी तरह विच्छिन्न। इन पाठों को भारतीय सांस्कृतिक विधाओं के सम्मिलन और टकराहटों के प्रमाण के रूप में देखा जाना चाहिए। इनका विश्लेषण मनुष्य, विशेषकर स्त्री आचरण-संहिताओं की दृष्टि से किया जाना चाहिए।
2. इन आचरण-पुस्तकों के समानांतर स्त्रियों के गद्य-लेखन की अंतर्वस्तु का विश्लेषण जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि अब तक विलुप्त और उपेक्षित (स्त्री-गद्य) से संबंधित परम्परा की विस्मृत कड़ियाँ भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक सूत्र में कैसे पिरोती हैं। साथ ही इसका अंदाजा भी लग सके कि तत्कालीन स्त्री-रचनाकार स्त्री, समाज, जेण्डर के विषय में क्या और कैसे सोचती थीं और वे गद्य में कैसे आचरण-संहिताओं का प्रतिरोधी विमर्श प्रस्तुत करती हैं।
3. प्रारम्भिक उपन्यासों की अर्थच्छटाओं को समझने के लिए औपन्यासिक परिदृश्य को समग्रता में देखे जाने की जरूरत है़। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के गद्य में साहित्य-रूपों और कथ्य की भिन्नता के बावजूद एक ही जैसे कथानक का दोहराव यह बताता है कि राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सांस्कृतिक मूल्यों और राजनीतिक उद्देश्य की भूमिका प्रमुख थी।
नवजागरण के दौर के लेखक भूमिका या प्रस्तावना में पुस्तक-लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया करते थे। मसलन 1869 में डिप्टी नजीर अहमद ने अपने समुदाय की स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए लिखे मिरात-उल-उरूस की भूमिका में उल्लेख किया था-
हम्द-ओ नात के बाद वजह हो कि हर चंद इस मुल्क में मस्तूरात के पढ़ाने-लिखाने का रिवाज नहीं, मगर फिर भी बड़े शहरों में खास-खास शरीफ खानदानों की बाज औरतें कुरान मजीद का तर्जुमा, मजहबी मसायल और नसायह के उर्दू रिसाले पढ़-पढ़ा लिया करती हैं। मैं देखता था कि हम मर्दों की देखा-देखी लड़कियों को भी इल्म की तरफ एक खास रगबत है। लेकिन इसके साथ ही मुझको यह भी मालूम होता था कि निरे मजहबी खयालात बच्चों की हालत के मुनासिब नहीं। और जो मजामीन उनके पेशे-नजर रहते हैं, उनसे उनके दिल अफसुर्दा, उनकी तबीयतें मुन्कबिज और उनके जहन कुंद होते हैं। तब मुझको ऐसी किताब की जुस्तजू हुई जो इखलाक और नसायह से भरी हुई हो और उन मामलात में जो औरतों की जिन्दगी में पेश आते हैं और औरतें अपने तोहमात और जहालत और कजराई की वजह से हमेशा इनमें मुब्तिला-रंज-ओ-मुसीबत रहा करती हैं, उनके खयालात की इस्लाह और उनकी आदात की तहजीब करे और कि दिलचस्प पैराये में हो जिससे उनका दिल न उकताए, तबीयत न घबराए। मगर तमाम किताब खाना छान मारा ऐसी किताब का पता न मिला, पर न मिला। तब मैंने इस कजिस्से का मंसूबा बाँधा।
Renaissance, Women’s Questions and Practices Books
इस पुस्तक को अंग्रेज शिक्षाधिकारी द्वारा एक हजार रुपये का पुरस्कार भी मिला था (इत्तेफाक से इसका मसौदा अंग्रेज डायरेक्टर तालीमात की नजर से गुजरा। वह इसे पढ़ कर फड़क उठा। उसी की तवज्जो से यह किताब छपी और इस पर मुसन्निफ को हुकूमत की तरफ से एक हजार रुपया इनाम मिला।)
हिंदी के प्रथम उपन्यास देवरानी-जेठानी की कहानी (1870) की भूमिका में भी पुस्तक-लेखन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गौरीदत्त शर्मा ने लिखा था-
स्त्रियों को पढ़ने-पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गयी हैं, सब अपने-अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नये रंग-ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री-पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएँगे। स्त्रियों का समय किस-किस काम में व्यतीत होता है। और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है, उसमें क्या-क्या हानि होती है। पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या-क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गयीं मैंने खोज कर सब लिख दी हैं। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम़ केमसन साहिब, डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस बहादुर को ऐसी पसंद आयी, मन को भायी और चित्त को लुभाई कि शुद्घ करके इसके छपने की आज्ञा दी और दो सौ पुस्तक मोल लीं और श्रीमन् महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नवम्बर 2672 लिखी हुई 24 जून, 1870 के अनुसार, इस पुस्तक के कर्ता पण्डित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले।
यह वह समय था जब गद्य-साहित्य के जरिये एक नये ढंग का सामाजिक और राजनीतिक सुधार आगे बढ़ाया जा रहा था। विभिन्न भारतीय भाषाओं में पश्चिम के प्रभाव और देशज आख्यान परम्परा के प्रभाव का सम्मिलित रूप गद्य में दिखाई दे रहा था। (उपन्यास) पद का प्रयोग अपने-अपने राजनीतिक-सामाजिक एजेण्डों की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में अलग-अलग साहित्य-रूपों में गद्य लिखा जा रहा था। लेकिन सांस्कृतिक और प्रांतीय साहित्य-रूपों और कथ्य की भिन्नता के बावजूद हमें एक ही जैसे कथानक का दोहराव दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सांस्कृतिक मूल्यों और राजनीतिक उद्देश्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुनर्जागरण के दौर में लिखे प्रारम्भिक गद्य को इस नये साहित्यिक जन के लिखित दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है।
Renaissance, Women’s Questions and Practices Books
उपन्यासकारों ने पश्चिमी शिक्षा तथा पारम्परिक संस्कृति और भारतीय धार्मिक-सामाजिक मूल्यों के तनाव और द्वंद्व की समस्या का सामना भी किया और ऐसी रचनाएँ औपनिवेशिक अनुभव के प्रतिरोध को दर्ज कराने और उनके वैचारिक अंतर्विरोधों का प्रमाण बन कर सामने आयीं। औपनिवेशिक सत्ता द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों और प्रशस्तियों ने भी लेखकों को प्रेरणा दी। मुंशी कल्याण राय और मुंशी ईश्वरी प्रसाद के सह-लेखन में प्रकाशित वामा शिक्षक की भूमिका में कहा गया-
इन दिनों मुसलमानों की लड़कियों के पढ़ने के लिए तो एक-दो पुस्तकें जह्यसे मिरात-उल-उरूस आदि बन गयी हैं, परंतु हिंदुओं व आर्यों की लड़कियों के लिए अब तक कोई ऐसी पुस्तक देखने में नहीं आयी, जिससे उनको जैसा चाहिए वह्यसा लाभ पहुँचे और पश्चिम देशाधिकारी श्रीमन्महाराजाधिराज लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर की यह इच्छा है कि कोई पुस्तक ऐसी बनाई जाए कि उससे हिंदुओं व आर्यों की लड़कियों को भी लाभ पहुँचे और उनकी शासना भी भली-भाँति हो। सो हम ईश्वरी प्रसाद मुदर्रिस रियाजी और कल्याण राय मुदर्रिस अव्वल उर्दू मदरसह दस्तूर तालीम मेरठ ने बड़े सोच-विचार और ज्ञान-ध्यान के पीछे दो वर्ष में इस पुस्तक को उसी ध्यान से बनाई। निश्चय है कि इस पुस्तक से हिंदुओं की लड़कियों को हिंदुओं की रीति-भाँति के अनुसार लाभ पहुँचे और सुशील हों और जितनी (बुरी) चालें और पाखण्ड जिनका आजकल मूर्खता के कारण प्रचार हो रहा है उनके जी से दूर हो जाएँगे और बुरी प्रवृस्त्रियों को छोड़कर अच्छी प्रवृस्त्रियाँ सीखेंगी और पढ़ने-लिखने और गुण सीखने की रुचि होगी़….
हिंदी के आरम्भिक दौर के सभी उपन्यासों के केंद्र में स्त्री-प्रश्न रहा है़ देवरानी-जेठानी की कहानी, भाग्यवती, वामा शिक्षक और एक सीमा तक परीक्षा गुरु में स्त्रियाँ ऐसे चरित्र के रूप में सामने लाई गयीं जिनके माध्यम से तत्कालीन समाज-व्यवस्था में सुधार की सम्भावना दिखाई पड़ती थी। इसी क्रम में (जेण्डर) को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखे गये। बावजूद इसके कि (जेण्डर) एक सामाजिक निर्मिति है जो किसी विशिष्ट व्यवहार का बारम्बार दोहराव होती है, इन उपन्यासों में जेण्डर को ले कर एक बँधी-बँधाई सोच दिखाई देती है भाषा कोई भी हो,अच्छी स्त्री के बरअक्स बुरी स्त्री का विलोम खड़ा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मिरात-उल-उरूस, देवरानी-जेठानी की कहानी और वामा शिक्षक जैसी पुस्तकें एक ही एजेण्डे के तहत रची गयीं। नजीर अहमद का उपन्यास दिल्ली के एक खाते-पीते मुसलमान परिवार की कथा कहता है, वहीं देवरानी-जेठानी की कहानी मेरठ के रूढ़िवादी बनिया परिवार की कहानी है दोनों की समानताएँ आश्चर्य चकित कर देने वाली हैं। दोनों में दो बहनें हैं जिनका एक ही परिवार के दो भाइयों से विवाह हुआ है। बड़ी बहू स्त्री की (स्टीरियोटाइप) अनपढ़ छवि का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने पति और श्वसुर की अवहेलना करती है, उनके सुझाव नहीं मानती और गहनों-कपड़ों की फरमाइश करती है जिसकी परिणति परिवार के विखण्डन में होती है। जबकि उसी की छोटी बहन योग्य, साक्षर, समझदार है, चतुराई से कम खर्च में घर-गृहस्थी चलाती है। दोनों जगह छोटी बहुएँ महान और सहनशील हैं। पतियों को सत्पथ पर लौटा ले आती हैं। ये सुधारकों की कल्पना की आदर्श स्त्रियाँ हैं जिनके चरित्र की चमक, अनपढ़, कुटिल और फूहड़ स्त्रियों के बरअक्स और अधिक चौंधियाती है। लेखक समाज के लिए अपेक्षित और काम्य स्त्री का प्रतीक रचते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें यह तो मालूम था कि राष्ट्र और समाज को कैसी स्त्री चाहिए, लेकिन यह नहीं पता था कि स्त्री को क्या चाहिए। डिप्टी नजीर अहमद का मानना था कि यदि एक स्त्री अपने पति की सेवा ठीक से करे, अपनी संतान और परिवार की योग्य देखभाल करे तो वह अपने समुदाय और राष्ट्र की सेवा कर सकती है। साथ ही, यह भी कि अपनी दुर्दशा के लिए स्त्रियाँ स्वयं उत्तरदायी हैं गुणों और सद्आचरण-द्वारा ही वे अपनी स्थिति में परिवर्तन और सुधार ला सकती हैं।
Renaissance, Women’s Questions and Practices Books
उन्नीसवीं सदी के इस दौर की राजनीति में ‘स्त्री-प्रश्न‘ उभार पर था और राजनीति और जेण्डर दोनों परस्पर असम्बद्ध नहीं, बल्कि कई स्तरों पर सम्बद्ध दिखते हैं पश्चिमी रहन-सहन के साथ औपनिवेशिक जीवन-शैली के संघर्ष और स्त्री प्रश्न पर वैचारकि अंतराल ने रचनाकारों को टकराने- जूझने तथा इसे अपना राजनीतिक एजेण्डा बनाने का अवसर दिया़। उदाहरण के लिए कन्नड़ के पहले कहे जाने वाले उपन्यास इंदिराबाई (1899) की चिन्ता के केंद्र में बाल-विवाह जैसी अहितकर सामाजकि प्रथाएँ हैं। गुलवाडी वेंकटराव उपन्यास में पाठकों के चरित्र-सुधार संबंधी उपदेश देते हुए लिखते हैं- ‘पाठक इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य पूछ सकते हैं। सच्चाई और हृदय की पवित्रता ही इहलोक और परलोक में सार्थकता दे सकती है। यह पुस्तक इसी बात को प्रमाणित करने के लिए लिखी गयी है।
इसमें इंदरिाबाई अंग्रेजी पढ़ी-लिखी युवती हैं, जो अपनी माँ अंबाबाई द्वारा प्रस्तावित राधाविलास जैसी भक्ति-श्रृंगार की पुस्तकें पढ़ने से मना करने पर अंग्रेजी की आचरण-पुस्तकें पढ़ती है। गुलवाडी वेंकटराव इंदिराबाई के रूप में आदर्श भारतीय स्त्री का चरित्र रचते हैं, जो विवाह और परिवार-संस्था में स्त्री की दोयम स्थिति पर कई प्रश्न-चिह्न खड़ा नहीं करती बल्कि किताबें पढ़ कर एक आदर्श आधुनिक घरेलू स्त्री बनने की दिशा में अग्रसर होती है। स्त्री की यह छवि पूरी तरह पुरुष-दृष्टि से निर्मित है। इस छवि का निर्माण करने में आचरण-पुस्तकों की भूमिका बहुत बड़ी थी। भारत में नीति-उपदेश की आख्यान परम्परा तो चली आ ही रही थी, पश्चिम में भी ‘आचरण-साहित्य’ का लेखन पुनर्जागरण काल में अपने पूरे उठान पर था। यह साहित्यिक नागरिकों के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश देता था। उच्च एवं मध्यवर्ग में मुद्रण प्रौद्योगिकी ने ऐसी पुस्तकों को लोकप्रिय बनाया। सोलहवीं शताब्दी में यद्यपि कई पुस्तकों के छपने पर पाबंदी लगी, लेकिन ऐसी आचरण-पुस्तकें सुरक्षित रहीं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लिखी गयीं। पुनर्जागरण के दौरान मानवतावादी विचारधारा ने व्यक्तिगत और सामाजकि आचार तथा शिक्षा के बीच संबंध कायम करने का प्रयास किया। सेंट क्लेयर ने कहा कि अच्छी शिक्षा व्यवहार सिखाती है तथा गम्भीर और उदात्त व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी होती है।
धीरे-धीरे ‘कंडक्ट’ या आचरण-साहित्य का केंद्रीय विषय स्त्रियाँ बनने लगीं। इनमें स्त्री के प्राथमिक कर्तव्य,पतिव्रत-धर्म, धर्म-पालन की शिक्षा और परिवार, सगे-सम्बन्धियों से व्यवहार के दिशा-निर्देश दिये जाने लगे। 1523 में जुआन लुईस वाइव्स ने एजुकेश्न ऑफ़ ए क्रिश्चियन वुमॅन शीर्षक पुस्तक में जीवन के तीन महत्वपूर्ण पड़ावों अविवाहिता, विवाहिता और विधवा के अनंतर स्त्री के व्यवहार के बारे में लिखा- ‘इन तीनों पड़ावों में स्त्री को अपनी पवित्रता और शुचिता का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए, इसे पुस्तक में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। पवित्र स्त्रियों को इस पुस्तक में अत्यंत विनम्र सुझाव दिये गये हैं।
ऐसी पुस्तकों का उद्देश्य स्त्री के शरीर और मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था, जिनके प्रकाशन में, पुनर्जागरण-काल में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई दी, इसलिए पुनर्जागरणकालीन यूरोपीय स्त्री पर टिप्पणी करते हुए पीटर स्टैली ब्रास ने कहा, ‘उसका शरीर बंदी है, उसका मुँह सिल दिया गया है और सिर्फ घर की चहारदीवारी के भीतर चलती-फिरती है। सभी आचरण-पुस्तकों का सुर एक ही है। उनमें वर्ग के आधार पर स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं है। लेखकों का मानना है कि वर्ग और जाति से परे स्त्री की शासना अनिवार्य है।
Renaissance, Women’s Questions and Practices Books
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें