उत्तरा का कहना है।
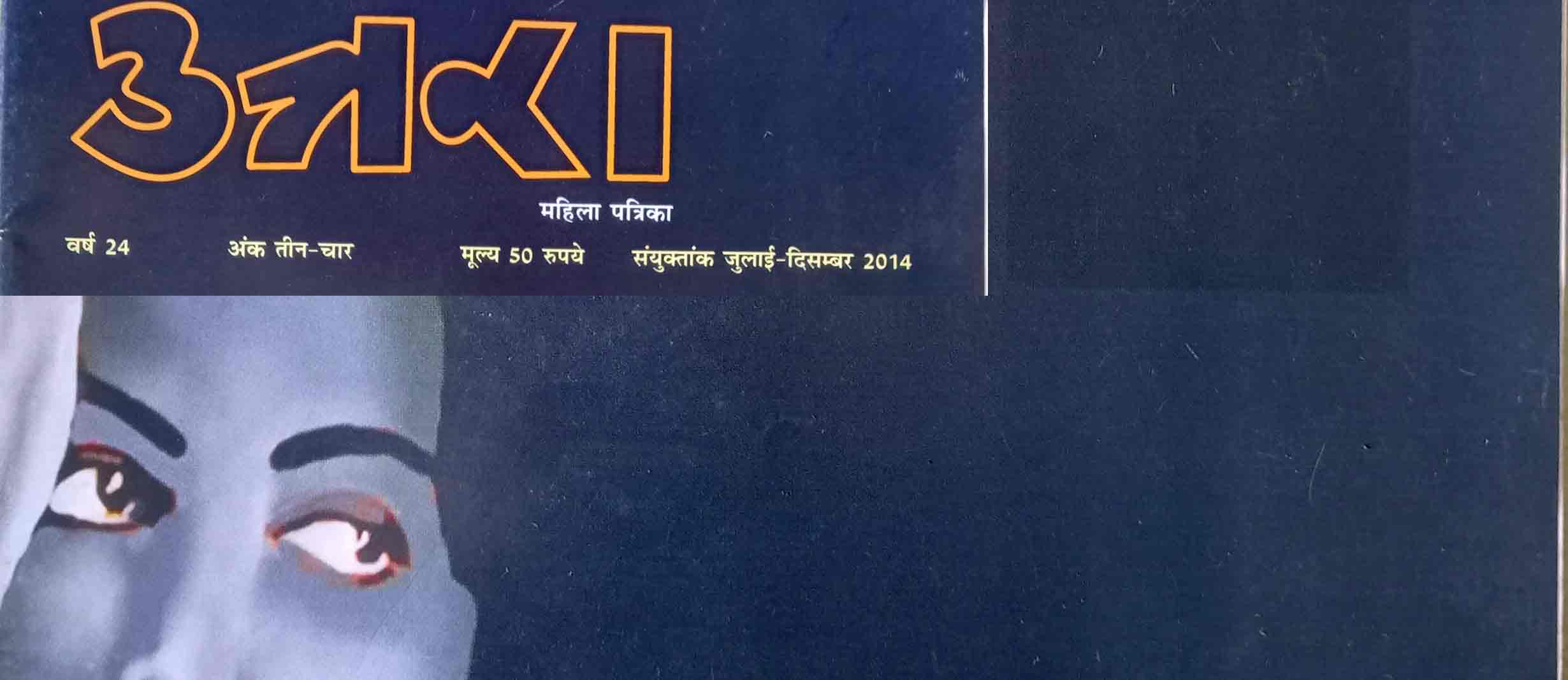
लोकसभा चुनाव 2014 भी हो गये और सत्ता में भाजपा आ गई। बहुत से लोगों को लग रहा था अगर मोदी सरकार आई तो बहुत कुछ बदल जायेगा नारा भी था अच्छे दिन आने वाले हैं। नारा इतना लुभावना था कि बच्चे-बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। वैसे ऐसी ही गेयात्मकता कांग्रेस के नारे- ‘हर हाथ तरक्की हर हाथ काम’ में भी थी। देखा जाय तो कांगे्रस का नारा ज्यादा जमींनी था। लेकिन अच्छे दिनों का जादू अधिक लोक-लुभावन रहा और जनता ने अच्छे दिनों के पक्ष में अपना पूर्ण बहुमत दे दिया। शायद अच्छे दिनों का नारा देने वालों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके पास अच्छे दिनों का कोई ठोस एजेण्डा था नहीं। जो फैसले अभी तक लिये गये हैं, उनमें जनता के लिये कोई भी अच्छे दिनों का संकेत देने वाले नजर नहीं आये। जनता के प्रति जवाबदेही का एक ही सूत्रवाक्य था- ‘यह तो पिछली सरकार का ही फैसला था’। हाँ, जो योजनायें पहले से चली आ रही थीं उन्हें जरूर अपने नाम जोड़े जाने की कवायद शुरू हो गई। जनता फिर से छली गई।
यह एक समय सत्य है कि विकास तो होगा ही, हर दिन कुछ नया भी होगा। मनुष्य की जिज्ञासा नई-नई खोज करेगी, आवश्यकतायें नये आविष्कार करायेगी। मनुष्य की सहज बुद्घि आराम, मनोरंजन और सुविधाओं के साधन जुटाने के लिये प्रेरित करेगी। सत्ता पाते ही उसके मन की भावनायें दया, माया, ममता का भाव रखकर कल्याण पथ को अपनायेंगी या लालच, झूठ और फरेब का मकड़लाल बुनेंगी, यह समझना बहुत आसान भी है और कठिन भी। आसान इसलिये कि आज की व्यवस्था कुछ ऐसी ही नुमाइंदगी पेश कर रही है। सब कुछ एकदम सामने है। कठिन इसलिये क्योंकि जिस तरह लोकलुभावन वायदों ने आकर्षित किया था, अब उनका इंतजार लाजिमी लग सकता है। अब मोदी सरकार कड़वी दवा का जुमला पेश कर फिर से अच्छे दिनों के इंतजार के लिए लोगों को तैयार कर रही है, उस पर बल देने के लिए पिछली सरकार के लम्बे शासनकाल की अव्यवस्थाओं की दुहाई दे दी जाती है। बहुत उम्मीद करना अपने को ही छलना होगा। अगर जनता ने भरोसा किया है तो उसका हक है कि वह अच्छे दिनों का इंतजार न करती रहे। पूर्ण बहुमत मिलने का मतलब मनमानी करने की छूट नहीं होना चाहिए। अगर जनता ने आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का हल नहीं मांगा तो वह सिर्फ सुनहरे ख्वाबों की दुनियां में सिमटकर रह जाएगी। 21वीं सदी में जाने, शाइनिंग इंडिया के नारे अभी जेहन में हैं लेकिन इनकी ताबीर नहीं हुई है।
दुनियां का सबसे बढ़ा लोकतंत्र है भारत। वोट देते समय यह लोक जरूर दिखाई देता है, दिखाई देता है अपनी पूरी ताकत के साथ। तंत्र भी पूरा-पूरा सक्रिय होता है। लेकिन चुनाव के बाद लोक अपने फौरी समाधान खोजने लगता है और तंत्र अपने रात्र अपने ही तौर तरीकों में नजर आने लगता है। हड़तालें होती हैं। अपने वेतन-भत्तों को बढ़ाने के लिए या नौकरी में आरक्षण या नियमितीकरण की मांग को लेकर। मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर उठाये गए जनता के मुद्दों को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं इन आंदोलनों को कम्यूनिस्ट नहीं अब सीधे सीधे माओवादी करार दे दिया जाता है। आम जनता में यही भ्रम लगातार फैलाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये माओवादी पढ़े-लिखे और अनपढ़ दोनों ही होते हैं, इसमें पत्रकार और प्रोफेसर भी होते हैं, इनमें बच्चे भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। इनकी मांग अपनी जमीन पर अपने हक की होती है, जिन्हें सरकार इनके मुंह का निवाला छीनकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप देती है। इन माओवादियों को नक्सलवादी, आतंकवादी कहकर फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जाता है। पुलिस तथा अन्य सैन्य बलों को इनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। कई बार वे भी मारे जाते हैं जिनके राजकीय सम्मान का ढकोसला कर दिया जाता है और जनता के सामने उन्हें महिमामंडित कर जनता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर अपना पक्षधर बना लया जाता है। यह बात दीगर है कि जब उन्हें मिले गोल्ड मैडलों की कलई खुलती है, तब पता चलता है कि वह तो सोना क्या किसी धातु के भी नहीं हैं महज प्लास्टिक हैं। बी बी सी ।
uttara ka kahna hai
बाहुबली नेताओं के पास अपने हथियार होते हैं, दबंगों की फौज होती है और सरकारी सुरक्षा भी उन्हें ही मिलती है। वे और उनके परिवार सरकारी बंगलों में रहते हैं, अपने लिए घर भी बनाते हैं और ऐशगाहें भी, सरकारी भूमि पर कब्जा भी करते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इन आवासों को आसानी से छोड़ते भी नहीं। विरोधियों को खुलेआम जान से मारने और बेइज्जत करने की धमकियाँ भी दे डालते हैं और कई बार अंजाम भी दे डालते हैं। कई-कई मुकदमों से सजे-धजे चुनाव में खड़े हो जाते हैं। जीत भी जाते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता रहता है। सोलहवीं लोकसभा में हर तीसरा सांसद आपराधिक मामलों में आरोपी है। चुनाव जीतकर आये 541 सांसदों में से 186 ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई आपराधिक केस दर्ज है।
किसान विद्रोह करेगा तो मारा जाएगा। मजबूरी है इस लोकंतत्र में उसका रहनुमा कोई नहीं अपनी मेहनत की कीमत मांगेगा तो अपनी जमीन पर हक मांगेगा तो दो वक्त की रोटी और तन ढंकने के लिए कपड़े चाहेगा तो आतंकवादी कहलायेगा। सरकार बन गई है, लेकिन कमजोर मानसून का मुकाबला तो उसे ही करना है। क्या हमारे लोकतंत्र का लोक और तंत्र इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि हमारे देश में सरकारी भाषा का आतंकवाद उन्हीं इलाकों में क्यों है जहाँ देश का वह गरीब तबका रहता है, जिसके पास सरकारी नौकरी या सरकारी व्यवस्था के तहत रोजगार के साधन नहीं हैं। जिसके नाम पर बहुत सारी कल्याणकारी योजनायें बन तो जाती हैं पर या तो व्यावहारिक नहीं होतीं या फिर व्यवहार में नहीं आतीं।
इस समय चर्चा का विषय है- रेल किराये में वृद्घि का। हमेशा की तरह लोगों के लिए एक और अधिभार है। सरकार का तर्क है कि बेहतर सुविधाओं के लिये यह बढ़ोत्तरी जरूरी है। जनता को सोचना चाहिए उन्हें बेहतर सुविधा वाली रेल सेवा चाहिए या ….. वैसे इस या के कोई मायने नहीं हैं क्योंकि सरकार ने मान ही लिया है कि किराया बढ़ाना ही है। आखिर हमें विश्वस्तरीय रेलवे का सपना जो देखना चाहिए। इस प्रकरण से एक बड़ी अलग सी बात याद आती है, जब दूध वाले दूध देते हैं तब वह गुणवत्ता की बात करते हैं कुछ दिनों में शिकायत पर दूध का दाम बढ़ाकर अच्छा दूध देने का वादा होता है। दूध की बड़ी हुई कीमत तो कम नहीं होती पर दूध फिर पहले जैसा हो जाता है। अगर फिर शिकायत की तो फिर वही दाम की बढ़ोत्तरी पर गुणवत्ता का सिर्फ वादा और दावा। कुशल गृहिणी परिवार की नियमित आय में से ही अतिथियों का सत्कार भी करती है और घर-परिवार के आकस्मिक खर्चों को भी पूरा करती है। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो वह इसका भत्ता सरकार से नहीं माँग सकती। उसे तो अपने बजट में से ही यह काम चलाना होता है। भला सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं। क्या जनता पर वैसे ही कम कर हैं जो व्यवस्था चलाने के लिए सरकार को हर स्तर पर महंगाई बढ़ाने और हर मद से कीमत वसूल लेने की जरूरत होती है।
अगर राजनैतिक पार्टियां अपने चुनावी खर्चों में बेतहाशा पैसा न लगायें, अपनी सुरक्षा के लिये सरकारी गैर सरकारी फौज न खड़ी करें, विदेश से काले धन के साथ साथ तथाकथित संत महात्माओं के आश्रमों की सम्पत्ति को विकास कार्यों में लगाने की हिम्मत दिखायें तो क्या विकास का सपना जमीनी धरातल पर नहीं साकार हो जायेगा। राष्ट्र ओर राष्ट्रवाद की दुहाई देने के साथ क्या हम अपनी राष्ट्र की सम्पत्ति का वास्तविक आंकलन नहीं कर सकते? देश में ही जो काला धन है उसका क्या। हमारे देश के किसान इसलिये आत्महत्या करने को मजबूर हैं क्योंकि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की सामथ्र्य नहीं रखते और कर्ज में डूबे हैं। क्या सरकारें इस बात का अध्ययन कर सकती हैं कि इन किसानों का कर्ज कितना था, जिसकी वह अदायगी नहीं कर सकता था इसलिए उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उससे कितना ज्यादा बकाया बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर है, सरकारी भवनों का कितना टैक्स बकाया है। महंगाई से निपटने के लिए जो चिंतायें जाहिर की जा रही हैं वह कितनी सार्थक और आम आदमी के हित में हैं, यह एक गम्भीर मुद्दा है। एक ओर तो सरकार कहती है जमाखोरी के कारण महंगाई है और जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर आलू-प्याज के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए वह जनता को बताती है कि मंडी के दामों से खुदरा व्यापारी कितना लाभ ले रहा है। वह इसके लिए सरकारी और सरकारी मान्यताप्राप्त आउटलैट्स को इसका विकल्प मान रही है, उस खुदरा व्यापारी का क्या होगा, उसके रोजगार और परिवार का क्या होगा। मंडी में किसान को उसकी उपज का क्या भाव मिल रहा है।
अगर गुुणवत्ता की बात करनी है तो उस चरित्र की गुणवत्ता की बात करनी होगी जिसमें लोकतंत्र के खोल में लोक की लूट खसोट के बल पर ऐशगाहें बनती हों, आम आदमी का किराया-भाड़ा बढ़ाकर बुलेट ट्रेन का सपना देखा जाता हो। रोटी की लड़ाई लड़ने वालों को आतंकवादी कहा जाता हो। सैन्य बलों को असीमित अधिकार देते हुए आम जनता का कत्ल कराया जाता हो, महिलाओं का बलात्कार कराया जाता हो और सैनिकों की मौत को शहादत के ग्लैमर में लपेट कर जनभावनाओं को उद्वेलित कर आम जन को आम जन से अलग कर दिया जाता है। लोकतंत्र की वास्तविक तस्वीर यही है।
नई सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं, उसने बदलाव को वोट दिया है, बहुत से सपने देखे हैं। लेकिन अभी तक जनता के सपनों की ताबीर होना तो दूर उनका जिक्र भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। आज मीडिया में हर वक्त हर खबर के साथ मोदी का सपना जुड़ा होता है, विश्वस्तरीय सपना और संदेश यह होता है कि सपना भी बड़ा होना चाहिए। हम बचपन में कई बार लोगों से ब्रिटेन की राजकुमारी के इस कथन को सुनते आ रहे हैं जब उसने कहा था कि अगर रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। हिंदुस्तान की वह जनता जो खडे-खड़े सफर करती है, उसका सपना क्या हो सकता है। पाकिस्तान और चीनी घुसपैठ की नाकामी को रोकने की कारगर कोशिशों को करने की जगह उन्हें सबक सिखाने की भाषा बोलकर जनता की वाहवाही पाना तो आसान विकल्प है अपनी लोकप्रियता बनाने के लिये। लेकिन उन परिवारों का क्या जो चीन-पाकिस्तान युद्घों में बेसहारा हो गये। शहीदों के सम्मान के नाम पर बनाये ग्लैमर को भुनाने में कौन सी बहादुरी है। जिस अवाम के हित के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, उन्हें कितना याद रखा गया है। कुछ तमगे और आर्थिक सहायता कितने घावों को भर सकती है।
छ: माह का समय कम नहीं होता। अब जनता को अपने फैसले का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने मत का हिसाब मांगना चाहिए। आखिर सपने तो जनता के भी हैं और उन्हें छीनने का हक किसी को नहीं है किसी को भी नहीं है।
uttara ka kahna hai
उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें :Uttara Mahila Patrika
पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये :यहाँ क्लिक करें

































